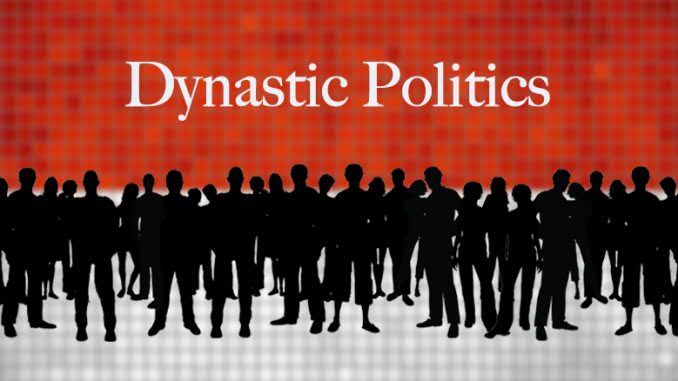जब भी राजनीति की बात होती है, तो एक शब्द अक्सर सुनाई देता है—वंशवाद या डाइनास्टिक पॉलिटिक्स। सवाल उठता है कि हमारे देश के सांसद (MPs), विधायक (MLAs), और विधानपरिषद सदस्य (MLCs) में कितने लोग वंशवादी राजनीति से आते हैं? यानी वो जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं, जिनके परिवार में अक्सर राजनीति का परंपरागत कब्जा रहता है। आज हम यही बात आम आदमी की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे।
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के कुल 5204 सांसदों, विधायकों और विधानपरिषद सदस्यों का लगभग 21% हिस्सा वंशवादी परिवारों से आता है। यानी लगभग हर पाँचवे विधायक या सांसद के पीछे कोई पुराना राजनीतिक परिवार जुड़ा होता है। लोक सभा में ये आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जहां 31% सांसदों का वंशवादी पृष्ठभूमि है। इसके मुकाबले राज्य विधानसभा में 20% और राज्य विधान परिषद में लगभग 22% वंशवादियों का दबदबा है।
आखिर यह वंशवादी राजनीति क्यों इतनी प्रबल है ? : –
इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये कि राजनीतिक प्रभाव और नाम की ताकत बहुत मायने रखती है। एक परिवार जिसने वर्षों से राजनीति में कदम रखा है, उसके संसाधन, नाम, नेटवर्क और वोट बैंक के कारण नए और गैर-वंशवादी नेताओं के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो जाता है। जब चुनाव होता है, तो जनता भी बड़े परिवारों के नाम से परिचित होने की वजह से उन्हें वोट देने का मन बनाती है।
ये भी पढ़े : – हेमंत सोरेन के संपत्ति का खुलासा: झारखंड के मुख्यमंत्री की दौलत की असली कहानी
राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस का वंशवाद सबसे ज्यादा है, जहां बाकी कुल सदस्यगण का लगभग 32% हिस्सा वंशवाद से जुड़ा है। भाजपा में यह आंकड़ा 18% है। वहीं माकपा (CPI-M) जैसी पार्टियां, जिनकी विचारधारा पारंपरिक राजनीतिक परिवारों से अलग होती है, उनमें यह चलन कम है, केवल 8%। राज्य स्तर की पार्टियों में नासिक के Sharad Pawar की NCP या जम्मू-कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों में वंशवादी राजनीति का दबदबा 30-40% तक देखा गया है।
राजनीतिक परिवारों की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में वंशवादी नेताओं की तादाद सबसे ज्यादा है। यूपी में कुल 604 नेताओं में से 141 (23%) और महाराष्ट्र में 403 नेताओं में से 129 (32%) का वंशवादी पृष्ठभूमि देखा गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी यह प्रतिशत काफी ऊंचा है।
एक दिलचस्प बात यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वंशवादी राजनीति का प्रभाव ज्यादा है। देश के 4665 पुरुष विधायकों में से 856 यानी लगभग 18% वंशवादी परिवारों से आते हैं, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा लगभग 47% है। इसका मतलब ज्यादा महिलाओं का राजनीतिक सफर वंशवादी परिवारों से ही शुरू होता है।
वंशवादी राजनीति के पक्ष और विपक्ष दोनों ही हैं। एक ओर यह राजनीति में एक तरह की निरंतरता और स्थिरता लाती है, जो अच्छे नेटवर्क और अनुभव का फायदा भी हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर, यह नई प्रतिभाओं के सामने रोक लगाता है, जो बिना पारिवारिक नाम के राजनीति में आना चाहते हैं। इससे लोकतंत्र की सच्ची प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है और पता नहीं किसे देखकर वोट देना सही रहेगा।
कई विशेषज्ञ इसके लिए आंतरिक पार्टी लोकतंत्र की कमी, सीमित अवसर और कुछ जनता की वंशवाद के पक्ष में झुकाव को जिम्मेदार ठहराते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह भारतीय राजनीति की विरासत है, जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, जहां परिवार इकाई का बहुत महत्व था।
ये भी पढ़े : – व्हाट्सएप मैसेज में जज पर आरोप लगाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का फैसला
आज की भारत में भी यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुई और भविष्य में इसे नियंत्रित करने के लिए आंतरिक सुधार और वोटर जागरूकता जरूरी है। सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय दलों में यह वंशवादी प्रभाव और भी जटिल रूप ले चुका है, खासकर राज्य राजनीति में।
तो इस कहानी का अंत करते हुए, यह कहा जा सकता है कि भारत की राजनीति में वंशवादी परिवारों की मौजूदगी स्थायी है, लेकिन साथ ही नई चुनौतियां और बदलाव दलों और जनता दोनों से आएंगे। आखिरकार, लोकतंत्र ऐसी जगह है जहां जनता का भरोसा और सचेत चुनाव ही तय करेंगे कि अगला नेता कौन होगा, चाहे वह परिवार से हो या नहीं।
(यह जानकारी हालिया 2025 की ADR और राष्ट्रीय चुनाव निगरानी रिपोर्ट पर आधारित है, जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की सचित्र तस्वीर पेश करती है)